निखिल अरोड़ा, नई दिल्ली: शायद हर कोई यह समझता है कि सोशल मीडिया और तकनीक में विश्वास पैदा करने की शक्ति होती है, जो सच साबित होने पर ही देखना को मिलती है। लेकिन मुझे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा मौका विरले ही देखने को मिला।
बैंक की तरलता में खतरे को लेकर हालिया विरोध चौंकाने वाला है, जो प्रस्तावित वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक के कारण हो रहा है।
एफआरडीआई विधेयक के संसद के पटल पर रखने के बाद एक अखबार के अभिमत-पृष्ठ पर ‘बैंकिंग ऑन लेजिस्लेशन’ के सरल शीर्षक के तहत पूरे तीन महीने तक प्रकाशित होने वाले आलेख से यह मुद्दा जोर पकड़ा है। खासतौर मसले को नाटकीय ढंग से व्हाट्सएप कवर नोट में बेल-इन क्लॉउज को ‘बैंकिंग आर्मगेडन एमेंडमेंट’ अर्थात बैंकिग क्षेत्र में बड़ा संशोधन के रूप में दर्शाया गया था।
जाहिर है कि सनसनीखेज की तरह मसले को प्रस्तुत करने का यह तरीका काम कर गया क्योंकि एक महीने बाद देश के वित्त मंत्री को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मसले को लेकर तीव्र सरगर्मियों को शांत करने की कोशिश की।
अब सही मायने में विधेयक का मूल्यांकन करने के लिए यह देखना होगा कि क्या मौजूदा मसौदे से जमाकर्ताओं के लिए बुरे दौर आनेवाले हैं। क्या विधेयक से यथास्थिति नाटकीय ढंग से बदल जाएगी? क्या आखिरकार इससे बेहतर या बदतर स्थिति पैदा होगी?
शेष दुनिया की तरह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भी जमा को बैंक के लिए ‘श्रेष्ठतम’ दायित्व के रूप में देखा जाता है और अंशधारकों (अर्थात शेयर अथवा निमायक पूंजी धारकों) की संपत्ति होने की स्थिति में ही घाटे का वहन किया जाता है और इसका अनुपालन साखकर्ताओं द्वारा किया जाता है और बुरे कर्ज के दौरान इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है।
इसलिए जमाकर्ताओं की संपत्तियों पर खतरा होने से पूर्व उनकी सुरक्षा कम से कम दो स्तरों होती है। इससे अलावा, सैंद्धांतिक रूप से सब कुछ समाप्त हो जाने की सूरत में भी जमा बीमा के तहत एक लाख रुपये की ‘सुरक्षा’ अनिवार्य है।
हालांकि नामुनासिब व चिंताजनक अत्यंत कम परिमाण में बीमाकृत जमा की बात सर्वथा अलग बहस की बात है।
व्यावहारिकता के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बतौर दूरदर्शी संस्थान के रूप में किसी भी बैंक की पूंजी अचानक निम्न स्तर पर आने पर हस्तक्षेप करेगा, जोकि जमाकर्ताओं की सुरक्षा का उच्चतम स्तर है।
अब 17 नवंबर के व्हाट्सएप संदेश पर विचार करें तो एफआरडीआई विधेयक में ऐसा अलग क्या है। शायद बहुत कुछ नहीं। सभी प्रकार के विधेयक पहले से मौजूद प्रक्रिया से ही तैयार किए जाते हैं। बीमाकृत जमा की सुरक्षा अभी भी अनिवार्य है। एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा में लचीली प्रक्रिया के जरिए बदलाव लाने का सुझाव दिया गया है जहां नव प्रकल्पित समाधान निगम द्वारा बीमाकृत रकम तय जाती है। इसका पुनरीक्षण काफी समय से लंबित था, क्योंकि 1993 में जब यह शुरू हुआ था तब इसका कोई मतलब नहीं था। इस प्रक्रिया को अब एक नाम दिया गया है- जोकि ‘बेल इन’ है, जोकि पाबंदी जैसा बन गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शब्द का प्रयोग होता रहा है।
जाहिर है कि व्यापक बीमा नेट के माध्यम से जमाकर्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए बहस की जा सकती है। लेकिन एफआरडीआई विधयेक लाने से लोगों की जमा पर खतरा बढ़ने का आरोप गलत है।
सही मायने में यह विधेयक एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि अनिश्चय की स्थिति पैदा होने पर जमाकर्ताओं के समाधान के लिए यह एक अलग व्यवस्था होगी जिस पर पहली पर विचार किया जा रहा है। यह बैंकों का व्यावसायिक मॉडल का हिस्सा है, जिसको अब संस्थागत बनाया जा रहा है और औपचारिक रूप से उसका नियमन किया जा रहा है।
सभी प्रकार के नियमनों से इतर जमाकर्ताओं कुछ स्तरों पर खतरों का सामना करना पड़ा है और हमेशा उन्हें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन बैंकिग तंत्र अब उस दिशा में काम कर रहा है। इसमें सबसे अहम बात स्वामित्व, उत्तरदायित्व और समाधान का मजबूत तंत्र सुनिश्चित करना है।
बाकी बातें बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण हैं।
( ट्रांसफिन के सीईओ व संस्थापक हैं और आलेख में उनके निजी विचार हैं)
–आईएएनएस




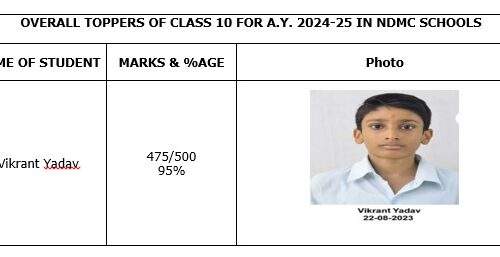




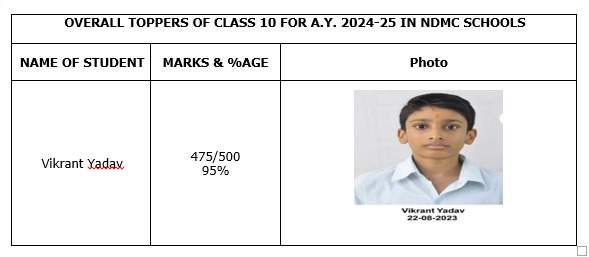
और भी हैं
दिल्ली : जेपी नड्डा ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की समीक्षा बैठक
सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों तैयार, देश में अन्न की कोई कमी नहीं : शिवराज सिंह चौहान
शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी हुईं भावुक, ‘सिंदूर का बदला लिया’